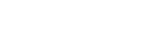एक तवाइफ़ का ख़त
पण्डित जवाहर लाल नेहरू और क़ाएद-ए-आज़म जिनाह के नाम
मुझे उम्मीद है कि इससे पहले आपको किसी तवाइफ़ का ख़त न मिला होगा। ये भी उम्मीद करती हूँ कि कि आज तक आपने मेरी और इस क़ुमाश की दूसरी औरतों की सूरत भी न देखी होगी। ये भी जानती हूँ कि आपको मेरा ये ख़त लिखना किस क़दर मायूब है और वो भी ऐसा खुला ख़त मगर क्या करूँ हालात कुछ ऐसे हैं और इन दोनों लड़कियों का तक़ाज़ा इतना शदीद हो कि मैं ये ख़त लिखे बग़ैर नहीं रह सकती। ये ख़त मैं नहीं लिख रही हूँ, ये ख़त मुझसे बेला और बतूल लिखवा रही हैं। मैं सिद्क़-ए-दिल से माफ़ी चाहती हूँ, अगर मेरे ख़त में कोई फ़िक़रा आपको नागवार गुज़रे। उसे मेरी मजबूरी पर महमूल कीजिएगा।
बेला और बतूल मुझसे ये ख़त क्यों लिखवा रही हैं। ये दोनों लड़कियां कौन हैं और उनका तक़ाज़ा इस क़दर शदीद क्यों है। ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको अपने मुताल्लिक़ कुछ बताना चाहती हूँ, घबराइए नहीं। मैं आपको अपनी घिनावनी ज़िंदगी की तारीख़ से आगाह नहीं करना चाहती। मैं ये भी नहीं बताऊंगी कि मैं कब और किन हालात में तवाइफ़ बनी। मैं किसी शरीफ़ाना जज़्बे का सहारा लेकर आपसे किसी झूटे रहम की दरख़्वास्त करने नहीं आई हूँ। मैं आपके दर्द मंद दिल को पहचान कर अपनी सफ़ाई में झूटा अफ़साना मुहब्बत नहीं घड़ना चाहती। इस ख़त के लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपको तवाइफ़ीयत के इसरार-ओ-रमूज़ से आगाह करूँ, मुझे अपनी सफ़ाई में कुछ नहीं कहना है। मैं सिर्फ़ अपने मुताल्लिक़ चंद ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जिनका आगे चल कर बेला और बतूल की ज़िंदगी पर असर पड़ सकता है।
आप लोग कई बार बंबई आए होंगे जिन्ना साहिब ने तो बंबई को बहुत देखा हो मगर आपने हमारा बाज़ार काहे को देखा होगा। जिस बाज़ार में मैं रहती हूँ वो फ़ारस रोड कहलाता है। फ़ारस रोड, ग्रांट रोड और मदनपुरा के बीच में वाक़े है। ग्रांट रोड के इस पार लेमिंग्टन रोड और ओपर हाऊस और चौपाटी मैरीन ड्राईवर और फोर्ट के इलाक़े हैं जहां बंबई के शुरफ़ा रहते हैं। मदनपुरा में इस तरफ़ ग़रीबों की बस्ती है। फ़ारस रोड इन दोनों के बीच में है ताकि अमीर और ग़रीब इससे यकसाँ मुस्तफ़ीद हो सकें। गौर फ़ारस रोड फिर भी मदनपुरा के ज़्यादा क़रीब है क्योंकि नादारी में और तवाइफ़ीयत में हमेशा बहुत कम फ़ासिला रहता है। ये बाज़ार बहुत ख़ूबसूरत नहीं है, इसके मकीन भी ख़ूबसूरत नहीं हैं उसके बेचों बीच ट्राम की गड़ गड़ाहट शब-ओ-रोज़ जारी रहती है। जहां भर के आवारा कुत्ते और लौंडे और शुह्दे और बेकार और जराइमपेशा मख़लूक़ उसकी गलियों का तवाफ़ करती नज़र आती है। लंगड़े, लूले, ओबाश, मदक़ूक़ तमाशबीन। आतिश्क व सूज़ाक के मारे हुए काने, लुंजे, कोकीन बाज़ और जेब कतरे इस बाज़ार में सीना तान कर चलते हैं। ग़लीज़ होटल, सीले हुए फ़ुटपाथ पर मैले के ढेरों पर भिनभिनाती हुई लाखों मक्खियां लकड़ियों और कोयलों के अफ़्सुर्दा गोदाम, पेशावर दलाल और बासी हार बेचने वाले कोक शास्त्र और नंगी तस्वीरों के दुकानदार चीन हज्जाम और इस्लामी हज्जाम और लंगोटे कस कर गालियां बकने वाले पहलवान, हमारी समाजी ज़िंदगी का सारा कूड़ा करकट आपको फ़ारस रोड पर मिलता है। ज़ाहिर है आप यहां क्यों आएँगे। कोई शरीफ़ आदमी इधर का रुख नहीं करता, शरीफ़ आदमी जितने हैं वो ग्रांट रोड के उस पार रहते हैं और जो बहुत ही शरीफ़ हैं वो मालबार हिल पर क़ियाम करते हैं। में एक-बार जिन्ना साहिब की कोठी के सामने से गुज़री थी और वहां मैंने झुक कर सलाम भी किया था, बतूल भी मेरे साथ थी। बतूल को आपसे (जिन्ना साहिब) जिस क़दर अक़ीदत है उसको मैं कभी ठीक तरह से बयान न कर सकूँगी। ख़ुदा और रसूल के बाद दुनिया में अगर वो किसी को चाहती हो तो सिर्फ़ वो आप हैं। उसने आपको तस्वीर लॉकेट में लगा कर अपने सीने से लगा रखी हो। किसी बुरी नीयत से नहीं। बतूल की उम्र अभी ग्यारह बरस की है, छोटी सी लड़की ही तो है वो। गो फ़ारस रोड वाले अभी से उसके मुताल्लिक़ बुरे बुरे इरादे कर रहे हैं मगर ख़ैर वो कभी भी आपको बताऊंगी। तो ये है फ़ारस रोड जहां मैं रहती हूँ, फ़ारस रोड के मग़रिबी सिरे पर जहां चीनी हज्जाम की दुकान है उसके क़रीब एक अँधेरी गली के मोड़ पर मेरी दुकान है। लोग तो उसे दुकान नहीं कहते, मगर ख़ैर आप दाना हैं आपसे क्या छुपाऊंगी। यही कहूँगी वहां पर मेरी दुकान है और वहां पर मैं इस तरह व्योपार करती हूँ जिस तरह बुनियाद, सब्ज़ी वाला, फल वाला, होटल वाला, मोटर वाला, सिनेमा वाला, कपड़े वाला या कोई और दूकानदार व्योपार करता है और हर व्योपार में गाहक को ख़ुश करने के इलावा अपने फायदे की भी सोचता है। मेरा व्योपार भी इसी तरह का है, फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि मैं ब्लैक मार्किट नहीं करती और मुझमें और दूसरे व्योपारियों में कोई फ़र्क़ नहीं। ये दूकान अच्छी जगह पर वाक़े नहीं है। यहां रात तो कुजा दिन में भी लोग ठोकर खा जाते हैं। इस अँधेरी गली में लोग अपनी जेबें ख़ाली कर के जाते हैं। शराब पी कर जाते हैं। जहां भर की गालियां बकते हैं। यहां बात बात पर छुरा ज़नी होती है वो एक ख़ूँ दूसरे तीसरे रोज़ होते रहते हैं। ग़रज़-कि हर वक़्त जान ज़ैक़ में रहती है और फिर मैं कोई अच्छी तवाइफ़ नहीं हूँ कि पवइ जा के रहूं या वर्ली पर समुंदर के किनारे एक कोठी ले सकूं । मैं एक बहुत ही मामूली दर्जे की तवाइफ़ हूँ और अगर मैंने सारा हिन्दोस्तान देखा है और घाट घाट का पानी पिया है और हर तरह के लोगों की सोहबत में बैठी हूँ लेकिन अब दस साल से इसी शहर बंबई में, इसी फ़ारस रोड पर, इसी दुकान में बैठी हूँ और अब तो मुझे इस दुकान की पगड़ी भी छः हज़ार रुपये तक मिलती है। हालाँकि ये जगह कोई इतनी अच्छी नहीं। फ़िज़ा मुतअफ़्फ़िन है, कीचड़ चारों तरफ़ फैली हुई है। गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और ख़ारिश-ज़दा कुत्ते घबराए हुए ग्राहकों की तरफ़ काट खाने को लपकते हैं फिर भी मुझे इस जगह की पगड़ी छः हज़ार रुपये तक मिलती है। इस जगह मेरी दुकान एक मंज़िला मकान में है। इसके दो कमरे हैं। सामने का कमरा मेरी बैठक है। यहां मैं गाती हूँ, नाचती हूँ, ग्राहकों को रिझाती हूँ, पीछे का कमरा, बावर्चीख़ाने और ग़ुस्लख़ाने और सोने के कमरे का काम देता है। यहां एक तरफ़ नल है। एक तरफ़ हंडिया है और एक तरफ़ एक बड़ा सा पलंग है और इसके नीचे एक और छोटा सा पलंग है और इसके नीचे मेरे कपड़ों के संदूक़ हैं, बाहर वाले कमरे में बिजली की रोशनी है लेकिन अंदर वाले कमरे में बिल्कुल अंधेरा है। मालिक मकान ने बरसों से क़लई नहीं कराई न वो कराएगा। इतनी फ़ुर्सत किसे है। मैं तो रात-भर नाचती हूँ, गाती हूँ और दिन को वहीं गाव तकिए पर सर टेक कर सो जाती हूँ, बेला और बतूल को पीछे का कमरा दे रखा है। अक्सर गाहक जब उधर मुँह धोने के लिए जाते हैं तो बेला और बतूल फटी फटी निगाहों से उन्हें देखने लग जाती हैं जो कुछ उनकी निगाहें कहती हैं। मेरा ये ख़त भी वही कहता है। अगर वो मेरे पास इस वक़्त न होतीं तो ये गुनाहगार बंदी आपकी ख़िदमत में ये गुस्ताख़ी न करती, जानती हूँ दुनिया मुझ पर थू थू करेगी , शायद आप तक मेरा ये ख़त भी न पहुँचेगा। फिर भी मजबूर हूँ ये ख़त लिख के रहूंगी कि बेला और बतूल की मर्ज़ी यही है।
शायद आप क़ियास कर रहे हों कि बेला और बतूल मेरी लड़कियां हैं। नहीं ये ग़लत है मेरी कोई लड़की नहीं है। इन दोनों लड़कियों को मैंने बाज़ार से ख़रीदा है। जिन दिनों हिंदू-मुस्लिम फ़साद ज़ोरों पर था, और ग्रांट रोड, और फ़ारस रोड और मदन पुरा पर इन्सानी ख़ून पानी की तरह बहाया जा रहा था। उन दिनों मैंने बेला को एक मुसलमान दलाल से तीन सौ रुपये के इवज़ ख़रीदा था। ये मुसलमान दलाल उस लड़की को दिल्ली से लाया था जहां बेला के माँ बाप रहते थे। बेला के माँ बाप रावलपिंडी में राजा बाज़ार के अक़ब में पुंछ हाऊस के सामने की गली में रहते थे, मुतवस्सित तबक़े का घराना था, शराफ़त और सादगी घुट्टी में पड़ी थी। बेला अपने माँ-बाप की इकलौती बेटी थी और जब रावलपिंडी में मुसलमानों ने हिंदूओं को तहे तेग़ करना शुरू किया उस वक़्त चौथी जमात में पढ़ती थी। ये बारह जुलाई का वाक़िया है। बेला अपने स्कूल से पढ़ कर घर आ रही थी कि उसने अपने घर के सामने और दूसरे हिंदुओं के घरों के सामने एक जम्म-ए-ग़फ़ीर देखा। ये लोग मुसल्लह थे और घरों को आग लगा रहे थे और लोगों को और उनके बच्चों को और उनकी औरतों को घर से बाहर निकाल कर उन्हें क़त्ल कर रहे थे। साथ साथ अल्लाहु-अकबर का नारा भी बुलंद करते जाते थे। बेला ने अपनी आँखों से अपने बाप को क़त्ल होते हुए देखा। फिर उसने अपनी आँखों से अपनी माँ को दम तोड़ते हुए देखा। वह्शी मुसलमानों ने उसके पिस्तान काट कर फेंक दिए थे। वो पिस्तान जिनसे एक माँ कोई माँ, हिंदू माँ या मुसलमान माँ, ईसाई माँ या यहूदी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और इन्सानों की ज़िंदगी में कायनात की वुसअत में तख़लीक़ का एक नया बाब खोलती है, वो दूध भरे पिस्तान अल्लाहु-अकबर के नारों के साथ काट डाले गए। किसी ने तख़्लीक़ के साथ इतना ज़ुल्म किया था। किसी ज़ालिम अंधेरे ने उनकी रूहों में ये स्याही भर दी थी। मैंने क़ुरआन पढ़ा है और मैं जानती हूँ कि रावलपिंडी में बेला के माँ-बाप के साथ जो कुछ हुआ वो इस्लाम नहीं था वो इन्सानियत न थी, वो दुश्मनी भी न थी, वो इंतिक़ाल भी न था, वो एक ऐसी सआदत, बेरहमी, बुज़दिली और शीतनत थी जो तारीख़ के सीने से फूटती है और नूर की आख़िरी किरन को भी दाग़दार कर जाती है। बेला अब मेरे पास है। मुझसे पहले वो दाढ़ी वाले मुसलमान दलाल के पास थी, बेला की उम्र बारह साल से ज़्यादा नहीं थी, जब वो चौथी जमात में पढ़ती थी। अपने घर में होती तो आज पाँचवीं जमात में दाख़िल हो रही होती। फिर बड़ी होती तो उसके माँ बाप उसका ब्याह किसी शरीफ़ घराने के ग़रीब से लड़के से कर देते, वो अपना छोटा सा घर बसाती, अपने ख़ाविंद से, अपने नन्हे-नन्हे बच्चों से, अपनी घरेलू ज़िंदगी की छोटी-छोटी ख़ुशियों से। लेकिन उस नाज़ुक कली को बे वक़्त ख़िज़ां आ गई, अब बेला बारह बरस की नहीं मालूम होती। उस की उम्र थोड़ी है लेकिन उसकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। उसकी आँखों में जो डर है, इन्सानियत की जो तल्ख़ी है या उसका जो लहू है मौत की जो प्यास है, क़ाइद-ए-आज़म साहिब शायद अगर आप उसे देख सकें तो उसका अंदाज़ा कर सकें। उन बे-आसरा आँखों की गहराइयों में उतर सकें। आप तो शरीफ़ आदमी हैं। आपने शरीफ़ घराने की मासूम लड़कियों को देखा होगा, हिंदू लड़कियों को, मुसलमान लड़कियों को, शायद आप समझ जाते कि मासूमियत का कोई मज़हब नहीं होता, वो सारी इन्सानियत की अमानत है। सारी दुनिया की मीरास है जो उसे मिटाता है, उसे दुनिया के किसी मज़हब का कोई ख़ुदा माफ़ नहीं कर सकता। बतूल और बेला दोनों सगी बहनों की तरह मेरे हाँ रहती हैं। बतूल और बेला सगी बहनें नहीं हैं। बतूल मुसलमान लड़की है। बेला ने हिंदू घर में जन्म लिया। आज दोनों फ़ारस रोड पर एक रंडी के घर में बैठी हैं।
अगर बेला रावलपिंडी से आई है तो बतूल जालंधर के एक गांव खेम करन के एक पठान की बेटी है। बतूल के बाप की सात बेटियां थीं, तीन शादीशुदा और चार कुंवारियां, बतूल का बाप खेम करन में एक मामूली काश्तकार था। ग़रीब पठान लेकिन ग़यूर पठान जो दियों से खेम करन में आ के बस गया था। जाटों के इस गांव में यही तीन चार घर पठानों के थे, ये लोग जिस हिल्म व आश्ती से रहते थे शायद उसका अंदाज़ा पंडित जी आपको इस अमर से होगा कि मुसलमान होने पर भी उन लोगों को अपने गांव में मस्जिद बनाने की इजाज़त न थी। ये लोग घर में चुपचाप अपनी नमाज़ अदा करते, सदियों से जब से महाराजा रणजीत सिंह ने अनान हुकूमत संभाली थी किसी मोमिन ने उस गांव में अज़ान न दी थी। उनका दिल इर्फ़ान से रोशन था लेकिन दुनियावी मजबूरियाँ इस क़दर शदीद थीं और फिर रवादारी का ख़्याल इस क़दर ग़ालिब था कि लब वा करने की हिम्मत न होती थी। बतूल अपने बाप की चहेती लड़की थी। सातों में सबसे छोटी, सबसे प्यारी, सबसे हसीन, बतूल इस क़दर हसीन है कि हाथ लगाने से मैली होती है, पंडित जी आप तो ख़ुद कश्मीरी-उल-नस्ल हैं और फ़नकार हो कर ये भी जानते हैं कि ख़ूबसूरती किसे कहते हैं। ये ख़ूबसूरती आज मेरी गंदगी के ढेर में गड-मड हो कर इस तरह पड़ी है कि इसका परख करने वाला कोई शरीफ़ आदमी अब मुश्किल से मिलेगा, इस गंदगी में गले सड़े मार दाढ़ी, घुन, मूंछों वाले ठेकेदार, नापाक निगाहों वाले चार बाज़ारी ही नज़र आते हैं। बतूल बिल्कुल अनपढ़ है। उसने सिर्फ़ जिन्ना साहिब का नाम सुना था, पाकिस्तान को एक अच्छा तमाशा समझ कर उसके नारे लगाए थे। जैसे तीन चार बरस के नन्हे बच्चे घर में 'इन्क़िलाब ज़िंदाबाद', करते फिरते हैं, ग्यारह बरस ही की तो वो है। अनपढ़ बतूल, वो चंद दिन ही हुए मेरे पास आई है। एक हिंदू दलाल उसे मेरे पास लाया था। मैंने उसे पाँच सौ रुपये में ख़रीद लिया। इससे पहले वो कहाँ थी, ये मैं नहीं कह सकती। हाँ लेडी डाक्टर ने मुझसे बहुत कुछ कहा है कि अगर आप उसे सुन लें तो शायद पागल हो जाएं। बतूल भी अब नीम पागल है। उसके बाप को जाटों ने इस बेदर्दी से मारा है कि हिंदू तहज़ीब के पिछले छः हज़ार बरस के छिलके उतर गए हैं और इन्सानी बरबरीयत अपने वहशी नंगे रूप में सब के सामने आ गई है। पहले तो जाटों ने उसकी आँखें निकाल लीं। फिर उसके मुँह में पेशाब किया, फिर उसके हलक़ को चीर कर उसकी ये आँतें तक निकाल डालीं। फिर उसकी शादीशुदा बेटीयों से ज़बरदस्ती मुँह काला किया। उसी वक़्त उनके बाप की लाश के सामने, रिहाना, गुल दरख़्शां, मरजाना, सोहन, बेगम, एक एक कर के वहशी इन्सान ने अपने मंदिर की मूर्तियों को नापाक किया। जिसने उन्हें ज़िंदगी अता की, जिसने उन्हें लोरियाँ सुनाई थीं, जिसने उनके सामने शर्म और इज्ज़ से और पाकीज़गी से सर झुका दिया था। उन तमाम बहनों, बहुओं और माओं के साथ ज़ना किया। हिंदू धर्म ने अपनी इज़्ज़त खोदी थी, अपनी रवादारी तबाह कर दी थी, अपनी अज़मत मिटा डाली थी, आज रिग वेद का हर मंत्र ख़ामोश था। आज ग्रंथ साहिब का हर दोहा शर्मिंदा था। आज गीता का हरा श्लोक ज़ख़्मी था। कौन है जो मेरे सामने अजंता की मुसव्विरी का नाम ले सकता है। अशोक के कत्बे सुना सकता है, एलोरा के सनमज़ादों के गुन गा सकता है। बतूल के बेबस भिंचे हुए होंटों, उसकी बाँहों पर वहशी दरिंदों के दाँतों के निशान और उसकी भरी हुई टांगों की नाहमवारी में तुम्हारी अजंता की मौत है। तुम्हारे एलोरा का जनाज़ा है। तुम्हारी तहज़ीब का कफ़न है। आओ आओ मैं तुम्हें इस ख़ूबसूरती को दिखाऊँ जो कभी बतूल थी। उस मुतअफ़्फ़िन लाश को दिखाऊँ जो आज बतूल है।
जज़्बे की रौ में बह कर मैं बहुत कुछ कह गई। शायद ये सब मुझे न कहना चाहिए था। शायद इसमें आपकी सुबकी है। शायद इससे ज़्यादा नागवार बातें आपसे अब तक किसी ने न की हों, न सुनाई होंगी। शायद आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। शायद थोड़ा भी नहीं कर सकते। फिर भी हमारे मुल्क में आज़ादी आ गई है। हिन्दोस्तान में और पाकिस्तान में और शायद एक तवाइफ़ को भी अपने रहनुमाओं से पूछने का ये हक़ ज़रूर है कि अब बेला और बतूल का क्या होगा। बेला और बतूल दो लड़कियां हैं, दो कौमें हैं, दो तहज़ीबें हैं। दो मंदिर और मस्जिद हैं। बेला और बतूल आजकल फ़ारस रोड पर एक रंडी के हाँ रहती हैं जो चीनी हज्जाम की बग़ल में अपनी दुकान का धंदा चलाती है। बेला और बतूल को ये धंदा पसंद नहीं। मैंने उन्हें ख़रीदा है। मैं चाहूँ तो उनसे ये काम ले सकती हूँ। लेकिन मैं सोचती हूँ मै ये काम नहीं करूँगी जो रावलपिंडी और जालंधर ने उनसे किया है। मैंने उन्हें अब तक फ़ारस रोड की दुनिया से अलग-थलग रखा है। फिर भी जब मेरे गाहक पिछले कमरे में जा कर अपना मुँह हाथ धोने लगते हैं, उस वक़्त बेला और बतूल की निगाहें मुझसे कहने लगती हैं, मुझे उन निगाहों की ताब नहीं। मैं ठीक तरह से उनका संदेसा भी आप तक नहीं पहुंचा सकती हूँ। आप क्यों न ख़ुद उन निगाहों का पैग़ाम पढ़ लें। पंडित जी मैं चाहती हूँ कि आप बतूल को अपनी बेटी बना लें। जिन्ना साहिब मैं चाहती हूँ कि आप बेला को अपनी दुख़्तर नेक अख़्तर समझें ज़रा एक दफ़ा उन्हें इस फ़ारस रोड के चंगुल से छुड़ा के अपने घर में रखें और उन लाखों रूहों का नौहा सुनिए। ये नौहा जो नवा खाली से रावलपिंडी तलक और भरतपुर से बंबई तक गूंज रहा है। क्या सिर्फ़ गर्वनमेंट हाऊस में इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, ये आवाज़ सुनेंगे आप।
आप की मुख़लिस
फ़ारस रोड की एक तवाइफ़
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.