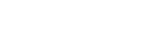रेख़्ता की कहानी
लफ़्ज़-ए-रेख़्ता, एक इस्तिलाह और इस्म-ए-ज़बान के तौर पर पिछली कई सदियों से इस्तिमाल हो रहा है। रेख़्ता के लुग़वी मानी ‘बिखरे हुए और मख़लूत के हैं’, जो इस ज़बान के मिज़ाज को ज़ाहिर करते हैं। लिसानियात के इलावा, मौसीक़ी में भी लफ़्ज़-ए-रेख़्ता अहम है। निस्फ़ सत्रहवीं सदी में मारूफ़ सूफ़ी अलाउद्दीन बरनवी ने अपनी तस्नीफ़ “चिश्तिया बहिश्तिया” में रेख़्ता की तारीफ़ मौसीक़ी की एक सिन्फ़ के तौर पर की है जिसमें फ़ारसी और हिन्दी के मिस्रे साथ गाए जाते हैं। तक़रीबन ऐसी ही रिवायत शायरी में भी मौजूद थी, जो आगे चल कर उर्दू शायरी के तौर पर ख़ूब फली फूली।
आज हम जिस ज़बान को उर्दू के नाम से पहचानते हैं, वो पिछले वक़्तों में मुख़्तलिफ़ नामों से जानी जाती रही है, जिनमें हिंदवी, हिन्दी, देहलवी, गुजरी, दकनी और रेख़्ता शामिल हैं। हम कह सकते हैं कि रेख़्ता ने अरबी-फ़ारसी अल्फ़ाज़ के साथ खड़ी बोली और ब्रजभाषा के इम्तिज़ाज से तैयार हो कर एक अदबी ज़बान के तौर पर अपनी पहचान क़ायम की है। इस के इर्तिक़ाई सफ़र पर ग़ौर करने से हमें मालूम होता है कि रेख़्ता ने मुख़्तलिफ़ ज़बानों से लिसानी और सक़ाफ़ती असरात क़ुबूल किए हैं। इसे लिखने के लिए शायर, सूफ़ी, हिंदू संत और सिख संत फ़ारसी के साथ-साथ नागरी, गुरमुखी, और कैथी रस्म-उल-ख़त का इस्तिमाल करते रहे हैं।
तेरहवीं सदी में, मश्हूर शायर अमीर ख़ुसरौ ने फ़ारसी और हिंदवी के इंतिहाई तख़्लीक़ी इम्तिज़ाज के साथ एक ग़ज़ल कही, जिस के अशआर में एक मिस्रा फ़ारसी और एक मिस्रा हिंदवी का है। उर्दू की पहली ग़ज़ल के तौर पर इसी ग़ज़ल का हवाला दिया जाता है।
ज़े-हाल-ए-मिस्कीं मकुन तग़ाफ़ुल दुराय नैनाँ बनाए बतियाँ
कि ताब-ए-हिज्राँ नदारम ऐ जाँ न लेहू काहे लगाए छतियाँ
शबान-ए-हिज्राँ दराज़ चूँ ज़ुल्फ़ ओ रोज़-ए-वसलत चूँ उम्र-ए-कोताह
सखी पिया को जो मैं न देखूँ तो कैसे काटूँ अँधेरी रतियाँ
यकायक अज़ दिल दो चश्म जादू ब-सद-फ़रेबम ब-बुर्द तस्कीं
किसे पड़ी है जो जा सुनावे पियारे पी को हमारी बतियाँ
चूँ शम-ए-सोज़ाँ चूँ ज़र्रा हैराँ ज़ मेहर-ए-आँ-मह बगश्तम आख़िर
न नींद नैनाँ न अंग चैनाँ न आप आवे न भेजे पतियाँ
ब-हक्क-ए-रोज़-ए-विसाल-ए-दिलबर कि दाद मारा ग़रीब 'ख़ुसरव'
सपीत मन के वराय रखूँ जो जा के पाऊँ पिया की खतियाँ
पंद्रहवीं और सोलहवीं सदी में रेख़्ता अभी एक नई ज़बान थी और सूफ़ी तसानीफ़ में इस के तख़्लीक़ी इस्तिमाल के कई नमूने मिलते हैं। सत्रहवीं सदी में वली ने अपनी शायरी से हर सुख़न-संज को हैरान कर दिया। वली की ग़ज़ल में फ़ारसी ग़ज़ल की रिवायत के साथ-साथ हिंदवी रिवायत के भी अनासिर मौजूद थे। वली की शायरी बेहद मक़बूल हुई और उसने दिल्ली के शुअरा को बहुत मुतअस्सिर किया और दिल्ली में भी रेख़्ता-गोई का रिवाज क़ायम हुआ। उस ज़माने में इन शाइरों के साथ साथ निर्गुन संत, कृष्ण भक्त, गुरु नानक की साखियों के मुसन्निफ़ीन ने भी रेख़्ता को अपने अदबी इज़्हार की ज़बान के तौर पर क़ुबूल किया।
अठारहवीं सदी में मीर तक़ी मीर ने रेख़्ता को अपनी शायरी के ज़रीए इस्तिहकाम और तवानाई बख़्शी। मीर ने लफ़्ज़-ए-रेख़्ता को शायरी के मानी में भी ख़ूब बर्ता है। मीर साहब ने हिंदवी और फ़ारसी के इम्तिज़ाज से बनने वाली छः अक़्साम का ज़िक्र किया है।
दिल किस तरह न खींचें अशआर रेख़्ते के
बेहतर किया है मैंने इस ऐब को हुनर से
मीर के हम-अस्र क़ाइम चाँदपूरी ने भी रेख़्ता को फ़ख़्र के साथ अपने अदबी इज़्हार की ज़बान के तौर पर चुना है।
‘क़ाइम’ मैं रेख़्ता को दिया ख़िलअत-ए-क़ुबूल
वर्ना ये पेश-ए-अह्ल-ए-हुनर क्या कमाल था
‘क़ाइम’ मैं ग़ज़ल तौर किया रेख़्ता वर्ना
इक बात लचर सी ब-ज़बान-ए-दकनी थी
नज़ीर अकबराबादी ने भी इस ज़बान को अपनाया:
यार के आगे पढ़ा ये रेख़्ता जा कर नज़ीर
सुनके बोला वाह-वाह अच्छा कहा अच्छा कहा
मुसहफ़ी ग़ुलाम हमदानी ने कहा है:
था जो शेर-ए-रास्त सर्व-ए-बोस्तान-ए-रेख़्ता
अब वही है लाल-ए-ज़र्द-ए- ख़िज़ान-ए-रेख़्ता
क्या रेख़्ता कम है मुसहफ़ी का
बू आती है इस में फ़ारसी की
यहाँ तक कि उर्दू के सबसे बड़े शायर मिर्ज़ा ग़ालिब ने इसमें मीर की उस्तादी का एतराफ़ किया है:
रेख़्ते के तुम्हीं उस्ताद नहीं हो ग़ालिब
कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था
इस के इलावा ग़ालिब ने रेख़्ता के बारे में कहा है:
तर्ज़-ए-बे-दिल में रेख़्ता कहना
असदुल्लाह ख़ाँ क़यामत है
जो ये कहे कि रेख़्ता क्यूँ के हो रश्क-ए-फ़ारसी
गुफ़्ता-ए-ग़ालिब एक-बार पढ़के उसे सुना कि यूँ
रेख़्ता मुग़ल दरबार में परवान चढ़ी, जहाँ उसे पहले ज़बान-ए-उर्दू-ए-मुअल्ला-ए-शाहजहाँबाद कहा जाता था। बाद में, इस नाम में तख़्फ़ीफ़ हुई और इसे ज़बान-ए-उर्दू मुअल्ला कहा जाने लगा। धीरे धीरे इसे ज़बान-ए-उर्दू, और आख़िर-ए-कार सिर्फ़ उर्दू कहा जाने लगा, और आज तक यही नाम राइज है। रेख़्ता, जो कि फ़ारसी और हिंदवी के इम्तिज़ाज से निकली थी, अब उर्दू की शक्ल में एक ताक़त-वर ज़बान का दर्जा हासिल कर चुकी है , और इसकी पहचान एक ऐसी ज़बान के तौर पर क़ायम हुई है जो शायराना कुव्वतों से मालामाल है और बेहद ख़ुश-सौत है।
रेख़्ता का इक्कीसवीं सदी का रूप उर्दू ही कहलाता है, जो हमारे मुशतर्का कल्चर की पैदा-वार है। आज रेख़्ता (उर्दू) हिन्दोस्तान, पाकिस्तान और जहाँ भी उर्दू बोली जाती है, के लिए हम-आहंगी और इत्तिहाद की सैकूलर ज़बान है।